बचपन का भी वो बहुत पहला और कच्चा सा हिस्सा था जब ना ‘सराय’ का मतलब पता था ना ही ये मालूम था कि ‘रोहिल्ला’ होता क्या है। उस वक़्त की यादें भी कैसे बची हैं ये सोच कर भी मैं हैरान हूँ । सराय रोहिल्ला स्टेशन से हमारा घर कुल तीन सौ मीटर पर था। घर के पास से बहुत सी रेल लाइन गुज़रती थी जिन पर से रेल आने और जाने के बाद कोयले के महीन कंकर हवा के साथ तीसरी मंजिल तक चले आते थे। चार मंजिल इमारत में हमारा एक कमरे का छोटा सा घर था जिस में माँ-पिताजी के साथ (तब तक) हम दो भाई और एक बहन ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके थे। बचपन में तो ये भी पता नहीं होता कि ज़िंदगी होती क्या है। बस खेल, खाना और माँ के पल्लू का छोर पूरी दुनिया थी। खाने को वक़्त से मिल ही जाता था, खेल और धमाल की कमी नहीं थी, पड़ोसियों और उनके बच्चों की भरमार थी और नींद जम कर आती थी ।
सराय रोहिल्ला का इतिहास 17वीं शताब्दी की एक सराय और 19वीं शताब्दी के एक रेलवे स्टेशन से जुड़ा है, जिसका नाम मुगल गवर्नर के बेटे रूहुल्लाह खान के नाम पर रखा गया था। “रोहिल्ला” शब्द का प्रयोग उत्तर भारत में अफ़गानिस्तान से आने वाले पश्तून कबीलों और शासकों के लिए भी किया जाता है, जिनका जलवा 18वीं शताब्दी में पूरे जोर पर था। दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन की स्थापना 1872 में हुई थी जब दिल्ली से जयपुर और अजमेर तक मीटर-गेज लाइन बनाई जा रही थी। 1857 से दिल्ली शहर अंग्रेजों के कब्जे में था और सत्ता कंपनी साहब से महारानी के हाथ आ चुकी थी जो मुग़लों के शहर को नया रूप देना चाहती थी। शाहजहाँनाबाद शहर के ठीक बाहर स्थित, यह स्टेशन तब हरियाणा में रेवाड़ी, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जाने वाली मीटर-गेज ट्रेनों के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता था। दिल्ली जंक्शन (पुरानी दिल्ली) से सराय रोहिल्ला तक की लाइन दोहरी-ट्रैक वाली थी, जबकि सराय रोहिल्ला से रेवाड़ी तक का खंड बहुत सालों तक सिंगल-ट्रैक ही रहा। रेवाड़ी से, सिंगल-ट्रैक पाँच दिशाओं में अलग-अलग हो गए। आज, स्टेशन के दक्षिण-पश्चिम में अहाता ठाकुरदास है और उसके दूसरी ओर एक रेलवे कॉलोनी है। एक छोटा सा इलाका, जिसे आज भी ‘सराय रोहिल्ला’ कहा जा सकता है, वास्तव में स्टेशन से आधा किलोमीटर उत्तर-पूर्व में है।
बीस पच्चीस मकानों वाला सन 1960 का सराय रोहिल्ला आज बेतरतीब फैलती बस्ती हुआ जा रहा है जहां किसी भी जगह से सड़क पार करने में ही 15 से बीस मिनट लग जाते हैं । इस बार जब में उस तरफ गया तो बचपन के अपने घर और आस पास की गंदगी को देख मेरा मन बहुत उचाट हुआ। यहाँ रहने वाले जिन लोगों से भी मैंने बात की उनमें कोई भी खुश नजर नहीं आया। 62 वर्षीय चंद्रावती देवी ने यहाँ आए बदलावों पर अफसोस जताते हुए कहा, “जब मैं शादी के बाद यहाँ आई थी, तब यहाँ केवल 60 घर थे।” आज, सराय रोहिल्ला एक घनी बस्ती है, जहाँ एक तरफ झुग्गियों की कतारें नीची छतों वाले पक्के घरों में बदल गई हैं और दूसरी तरफ बेतरतीब इमारतों में छोटी-छोटी दुकानें और कारखाने चल रहे हैं।
सराय रोहिल्ला में जहां हम रहते थे वो बहुत बड़ी और ऊंची चौकोर इमारत थी जिसके अंदर चारों और कमरे ही कमरे थे, एक के बाद एक – लाइन वार । इन सब कमरों के सामने एक बरामदा खुलता था जो उस मंजिल के सभी कमरों को जोड़ता था। बरामदा करीब चार या पाँच फुट चौड़ा रहा होगा जिसकी दीवार भी टीन फुट से ऊंची थी, हम बच्चे उस दीवार तक पहुँच नहीं पाते थे ना ही देख पाते थे कि उसके बाद क्या है । इमारत के बीचों-बीच कुछ नहीं था – गहरा खालीपन, वो खालीपन जो नीचे तक उतरता था जहां बहुत बड़े चौक नुमा आँगन में एक कुआं था। वैसे तो हमारे कमरे और गुसल तक पानी की लाइन आती थी फिर भी कभी कभार जब पानी नहीं आता था तो बरामदे में खड़े हो कर हर घर वाला अपने लिए इसी कुआं का पानी ऊपर खींच लेता था। ऐसे दिन हम सब बच्चों के लिए बहुत रोमांचक होते थे। कोई ना कोई बड़ा हम बच्चों को कंधों पर या गोदी में उठाकर पानी खींचने का नज़ारा दिखा देता था और फिर खींची गई बाल्टी से पानी टब या दूसरी बाल्टी में पलटते हुए कुछ पानी गिर कर बिखर जाता था। भीगे हुए बरामदे में हम बच्चे उस रोज़ खूब स्केटिंग करते थे ।
एक दूसरे से उलझती, एक दूसरे का रास्ता काटती, कहीं सीधी, कहीं घूमती और आपस में चिपकी काले लोहे की इन रेल पटरियों को हम बच्चे बड़ी हैरानी और असमंजस से ताकते थे। इतनी सारी लाइनों को अपने अंदर समटे दो तरफ़ गिरने और उठने वाला फाटक भी अपने आप में अजूबा था। ये फाटक हाथ से चक्का चल कर उठाए और गिराए जाते थे । पूर्वी और पश्चिमी फाटक एक दूसरे से बहुत दूर थे जिनके कोने में टीन की छोटी झुग्गी में उन फाटकों को चालने वाले रहते थे जिनको मैंने सिवाय कच्छे और बनियान के कभी किसी और कपड़े में नहीं देखा था। हमारी तरफ वाला फाटक चलाने वाला कोयले सा काला इंसान अपने हाथ में दो झंडे पकड़े रहता था – एक लाल और एक हरा, वो हमेशा खाँसता मिलता था।
स्टीम इंजिन से चलने वाली रेल की लंबी सी पटरी से आता टका-टक का शोर और दूर तक फैलता सलेटी धुआँ हमे बचपन में परेशान नहीं करता था। हमारे कमरे के ऊपर भी एक और मंजिल थी जिसकी वजह से हम लोग रेल को सिर्फ सुन और महसूस कर पाते थे देख नहीं पाते थे। देखने को मिलते थे इंजिन के हवा में दागे कोयल के बारीक कंकड़। कोयले का बूरा, बारीक कंकड़, धूल और काली राख हमेशा विराजमान रहती थी। रेल स्टेशन के साथ साथ सराय रोहिल्ला पर कोयला और लोहे के सरिये आदि उतारने की साइडिंग भी थी। इसके साथ साथ था रेलवे का अपना कबाड़घर। प्लेटफॉर्म के आगे कोयले और लोहा लँगड़ के बेशुमार ढेर बिखरे पड़े रहते जहां से ट्रक और बैल गाड़ियां इन्हे ले कर जाती थीं।
हमारे कमरे के बाहर वाले बरामदे में दिन भर झाड़ू लगा कर सफाई करनी पड़ती थी। हम भाई-बहन इस सब में माहिर हो चले थे, झाड़ू बाहर ही रहता था, डालड़ा घी का एक पुराना खाली डिब्बा भी। काली धूल बीन कर उसे हम पास पड़ी अंगीठी में डाल देते। अंगीठी भी दिन भर जलती थी, उसके पास रखा होता था किरोसीन का स्टोव जो सिर्फ भगोने टिकाने के काम आता था। स्टोव बेचारे की किस्मत ही कुछ ऐसी थी। हमारी तरह वो भी महीने के दो हफ्ते मायूस ही पड़ा रहता था। पिता की तनख्वाह खत्म, किरोसीन खत्म, जोश खत्म। बेचारे के पेट में ही कुछ नहीं जाता था तो वो क्या काम करता। अंगीठी पे शायद अभिशाप था – दिन रात जलते रहने का ।
खैर, वापिस सराय रोहिल्ला पर।
सराय रोहिल्ला वाले कमरे में अपने माँ-पिता के साथ हमने शायद पाँच साल बिताए। ये चार मंज़िला बिल्डिंग न्यू रोहतक रोड पर दक्षिण को उतरती ढलान पर बनी थी जिस के दाहिने यानि पूरब की तरफ़ रेल लाइन थी जिसके फाटक बंद होने पर बाहर दोनों तरफ़ ताँगों, रिक्शों, बैल गाड़ियों और टेम्पो आदि का खासा जाम लगा रहता था। पश्चिम को आनंद पर्वत का फैक्टरी या छोटे कारखानों का ऊबड़ खाबड़ इलाका – उत्तर को ढलान लेती सड़क नजफ़गढ़ रोड और जखीरा पुल की तरफ जाती थी और दक्षिण में तिबिया कॉलेज से गुज़रती ईदगाह, सदर बाजार की ओर से पहाड़ गंज और कन्नाट प्लेस की तरफ़। उन दिनों सड़क पर ना के बराबर ट्राफिक रहता था । इक्का दुक्का कार या रोडवेज़ की बस – बाकी सब साइकिल, तांगे, हाथ रिक्शा, बैल गाड़ी या पैदल सवार। इन सब के चलने की स्पीड भी तकरीबन एक जैसी थी। तब सड़क पर घोड़े, खच्चर, ऊंट दौड़ाते लोग भी मिल जाते थे। शाम ढले पालकी ढोते सवार भी दिख जाते थे। दोपहर में भेड़ों का रेला रोज़ ही मिल जाता था ।
हमारी बिल्डिंग के बाहर उसका नाम लिखा था “यादव भवन” जिसके भू तल यानि ग्राउन्ड फ्लोर पर बाहर की तरफ पाँच दुकाने थीं । एक पंसारी, एक ढाबा, एक बजाज यानि कपड़े वाला, एक नाई और एक जो बिल्डिंग के मालिकों की अपनी दुकान थी उसके अंदर बाहर कपास के बड़े-बड़े गट्ठर और दाल की बोरियाँ रखी रहती थीं । इन दुकानों के बाद बिल्डिंग के अंदर जाने का रास्ता और उसके आगे ऊपर की मंजिलों तक पहुँचने वाली ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थीं । ज़ीने पर चढ़ने में हम बच्चों को बहुत मशक्त करनी पड़ती थी। सीढ़ी में अंधेरा रहता था, वहाँ बिजली का बल्ब तो लगा था पर उसकी बत्ती कभी जलती नहीं थी। हर मंजिल वाले एक लालटेन जला अपनी मंजिल की सीढ़ियों के आगे छोड़ देते थे।
तीसरी मंजिल पर हमारे साथ वाले कमरे में एक कश्मीरी परिवार रहता था, कोई कौल साहब थे जिनकी पत्नी अपने कानों में लंबे लंबे धागों वाले सोने के गहने पहनती थीं । उनके दो बच्चे थे एक लड़का और एक लड़की । लड़के का नाम तो मुझे याद नहीं पर उस गोरी चिटटी, लाल गालों वाली खूबसूरत लड़की का नाम था अड़िमा – बहुत मीठा और धीमा बोलती थी अड़िमा – उसे ठीक सुन पाने के लिए मुझे अक्सर अपना कान उसके मुहँ तक ले जाना पड़ता था। उसके मुहँ से गज़ब की महक आती थी, जाने क्या चबाती थी। हमारे साथ दूसरी तरफ एक नागपाल दंपति रहता था जिनका कोई बच्चा नहीं था। नागपाल आंटी मुझे बहुत प्यार करती थीं और हर रोज़ कुछ खाने को देती थीं, अकेली वही मेरे जन्मदिन पर तोहफ़ा लाती थीं । नागपाल अंकल के पास वेसपा स्कूटर था जिस पर बैठा कर उन्होंने मुझे कई बार सैर कराई। बाकि किसी और के बारे में ना मुझे याद है ना ही शायद हम किसी को जानते थे। हाँ, हमारे पिताजी हर इतवार हमे छत पर ले जा कर खूब तस्वीरें खींचते थे। वो कोडेक बॉक्स कैमरा मुझे आज भी याद है ।
दक्षिण से उत्तर को जाती न्यू रोहतक रोड के दाहिनी तरफ सराय रोहिला स्टेशन की लंबी दीवार थी जो किसी किले की पुराने दीवार सी लगती थी। हमारे वहाँ रहने के दौरान ही उस दीवार के साथ-साथ राजस्थान से आए खानाबदोश गडुलिया या गाड़िया लोहार कबीले अपनी खूबसूरत गाड़ियों के साथ आ कर रहने लगे, ऐसा माना जाता है कि गड़िया लोहार महाराणा प्रताप की प्रजा और वंशज हैं। लोहे के औज़ार, हथियार, बर्तन, और घर का सामान बनाने वाले ये गड़िया लोहार राजपूत बताए जाते हैं।
हट्टे-कट्टे, बलिष्ठ और मेहनती गाड़िया लोहार धधकती भट्टी या आग के सामने भारी भरकम हथोड़ों से लाल लोहे को पीटते और उसको नई शक्ल देते दिख जाते थे। इनकी औरतें भी उतनी जोर से हथोड़ा चलाती थी जितने इनके मर्द। कई गर्भवती औरतें भी आग के सामने चमड़े की धोकनी से आग को हवा देती दिख जाती थीं। बाकि औरतें बर्तन माँजती, रोटी बनाती और बच्चों को पालती थीं। इन औरतों में से किसी को मैंने शहरी औरतों की तरह दुबला पतला या मरियल सा नहीं देखा। गड़िया लोहारों के छोटे बड़े बच्चे दिन के किसी भी वक़्त रेल लाइनओं के आस पास मँडराते दिखाई पड़ते थे । लड़कों के हाथ में बोरियाँ होतीं और लड़कियों के सर पे पास बांस की टोकरिया। रेल कारांचारियों से नजर बचा कर ये बच्चे अपनी बोरियों और टोकरियों में कोयला और लोहे का कबाड़ इकट्ठा करते । पकड़े जाने पर कभी कभी तो इनकी खूब धुलाई होती ।
खैर, बचपन में ये सब मुझे परेशान नहीं करता था तब तो मैं सड़क किनारे चलता हुआ गाड़िया औरतों के काले कपड़े, उनकी बड़ी आँखों में काला काजल, रंगीन डोरियों वाली चोलियों और उनकी चांदी के गहनों से भर हाथ, पैर और गले देख कर अचंभित सा एक जगह जम जाता था। मेरी बड़ी बहन राधे बताती हैं की “कई बार ये औरतें तुझ छोटे कद के गोरे चिट्टे, गोल मटोल, प्यारे से लड़के को देख उठा लेती और मैं डर जाती थी”।
उनकी गाड़ियां छोटी-छोटी चीज़ों से सजी होती जैसे घुंघरू, घंटियाँ, शीशे की गोल बिंदियाँ, सजावटी धातु की प्लेटें और कपड़े की रंगीन झंडियाँ । इन गाड़ियों को चलाने वाले बैल मुझे कभी दिखाई नहीं दिए। ये गाड़ियाँ बांस की सिरकी से ढकी होती जो शायद उन्हें धूप और बारिश से बचाती थी। याद नहीं उन दिनों मच्छर होते थे कि नहीं । साल के बाकी महीनों में जब तेज गर्मी या हाड़ जमा देने वाली ठंड पड़ती होगी तब जाने ये लोग कैसे रहते होंगे।
वैसे तो हमारे वाले घर पर पक्की छत थी और चारों तरफ़ पक्की दीवारें थी फिर भी सर्दी गर्मी से हम भी परेशान ही रहते थे। गर्मी में दीवारें गरम और सर्दी में ठंडी हो जाने से कभी चैन तो नहीं मिलता था। बारिश में तो उस इलाके का हाल तो खासा खराब हो जाता था। चारों तरफ़ पानी जमा हो जाने से हमारी बिल्डिंग एक टापू सी हो जाती थी अगर कहीं बारिश दो तीन रोज चल जाती तो खाने पीने का सामान तक मिलना मुश्किल हो जाता। ऐसे व्यक्त में गाड़िया लोहारों की तो शामत आ जाती थी। बेचारे पूरे परिवार के साथ अपनी अपनी गाड़ी में फंस कर रह जाते।
गाड़िया लोहारों की गाड़ियों की बनावट आगे से घोड़ा या बैल गाड़ी सी होती है जिसमे आगे के हिस्से में जानवर बांध कर उसे खींच जा सकता है । बरसात के दिनों में इन परिवारों की औरतें इसके सामने वाले जोत पर चूल्हा जला कर बामुश्किल खाना बनाती। कुल मिला कर इन खानाबादोशों के लिए ज़िंदगी तब भी बहुत कठिन थी और आज भी है।
आज भी जब मैं महरौली वाली सड़क के किनारे इन्हे बसा देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि 21वीं सदी में भी हमारी सरकारें इन घुमक्कड़ कबीलों के लिए कुछ सुविधाएं क्यूँ नहीं जुटा पाती? पूरे उत्तरी भारत में ये लोग साल भर घूमते हैं हम क्यूँ नहीं इनके लिए नियत स्थान तय कर सकते जहां इनके लिए मूल भूत सुविधाएं हों। एक बड़ा सा खुला साफ़ मैदान हो जहां इन्हें साफ़ पानी और टॉइलेट मिले, जहां ये लोग चार छे महीने रुक कर अपने द्वारा बनाए माल को बेच अपना जीवन चला सकें? किसी सरकार के लिए ये कोई ज्यादा मुश्किल या खर्चीला काम तो नहीं है, बिल्कुल इसी तरह की सुविधाएं सरकार ने हथकरघा और दस्तकारों के लिए हर शहर में बनाई हैं, आखिर गड़िया लोहार भी तो लोहे का सामान बनाने वाले हस्तशिल्पी ही तो हैं ये भी अपने हाथ और अपनी मेहनत से सामान बनाते हैं।
अब तो ये लोग अपने साथ ढोंर डाँगर भी नहीं रखते। अब इनके पहनावे भी काफी हद तक शहरी हो गए हैं, खान-पान और रहन-सहन भी बदल चुका है। कुछ परिवारों ने तो अपनी पहचान यानि “लोहार गाड़ियां” भी त्याग दी हैं और अब सड़क किनारे टीन की चादर से ढके कच्चे कमरे से बनाकर रह रहे हैं । इन में से बहुत ने तो बिजली के कनेक्शन भी ले रखे हैं । तकरीबन हर झुग्गी नुमा घर में टेलिविज़न देखने वाली सैटेलाइट डिश भी लगी मिल जाती है। इनके युवा भी बाकी युवाओं की तरह मोबाईल फोन और इंटरनेट पर चलने वाली फूहड़ फिल्मों के आदि हो चुके हैं ।
हमारे बचपन के वक़्त से अब में फ़र्क सिर्फ इतना हुआ है कि तब हम इनके पड़ावों, इनकी गाड़ियों के पास जाकर इन्हें लोहे का सामान बनाते देख सकते थे, इनकी फौलादी ताकत और लोहे से कुछ भी बना लेने के इनके हुनर पर नाज़ करते थे और वो सामान फख्र से खरीद सकते थे पर आज ये परिवार वाले अपने छोटे छोटे बच्चों को चौराहे की लाल बत्ती पे सामान बेचने के लिए मजबूर हैं। इनके छोटे बच्चे सारा दिन धूल मिट्टी और धुएं के बीच अपनी सेहत खराब कर अपने घर के लिए चार पैसे जुटा पाते हैं और मोटरों मे बैठे शहरी लोग इनसे मोल भाव कर इनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। सिर्फ शहरी ही नहीं, चौराहे पर खड़े पुलिस वाले भी इनके साथ बुरा व्यवहार और छेड़ खानी करते हैं और इनसे हफ्ता भी वसूलते हैं। इनके कुछ युवा तो गलत धंधों में लग कर जीवन बर्बाद कर रहे हैं ।
बादशाह अकबर ने तो 1568 में चित्तौड़गढ़ किले पर कब्ज़ा करने के बाद मेवाड़ छोड़ ही दिया था। वो समय तो कभी का बीत चुका । क्या गाड़िया लोहार आज भी अपने राजा की शपथ से मुक्त नहीं हुए? कब तक भागेंगे ये लोग? महाराणा प्रताप तो अब लौटेंगे नहीं – अब तो ना वो राजा रहे ना वो देस, क्या ये कभी अपने वतन नहीं लौटेंगे? और अगर नहीं भी जाना तो ये गाड़िया किसी एक जगह के हो कर कहीं बस कीं नहीं जाते? बिना बैल की इन गाड़ियों को ले कर कब तक भटकते रहेंगे ये परिवार ? क्या इनका अपने बच्चों अपने परिवारों की तरफ़ कोई फर्ज नहीं है? इन सब सवालों का जवाब आसान नहीं है मैं ये जानता हूँ पर क्या एक देश को अपने वासियों के भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए? देश की जीडीपी में इनकी मेहनत भी गिनी जानी चाहिए ।
21वीं सदी की इस तरक्की और देश के विकास का हश्र क्या सिर्फ ये है कि हमारे जन जातीय कबीलों को अपनी निजी पहचान शहर के हाथों खोनी पड़ेगी? मेरा मानना है की अपने आदिवासियों, देशज और मूल निवासियों और अपनी संस्कृति वा सभ्यता का इतना बड़ा हिस्सा खोना हमे बहुत महंगा पड़ेगा।
राजिंदर अरोड़ा – 17 नवम्बर 2025 (2745 शब्द)

















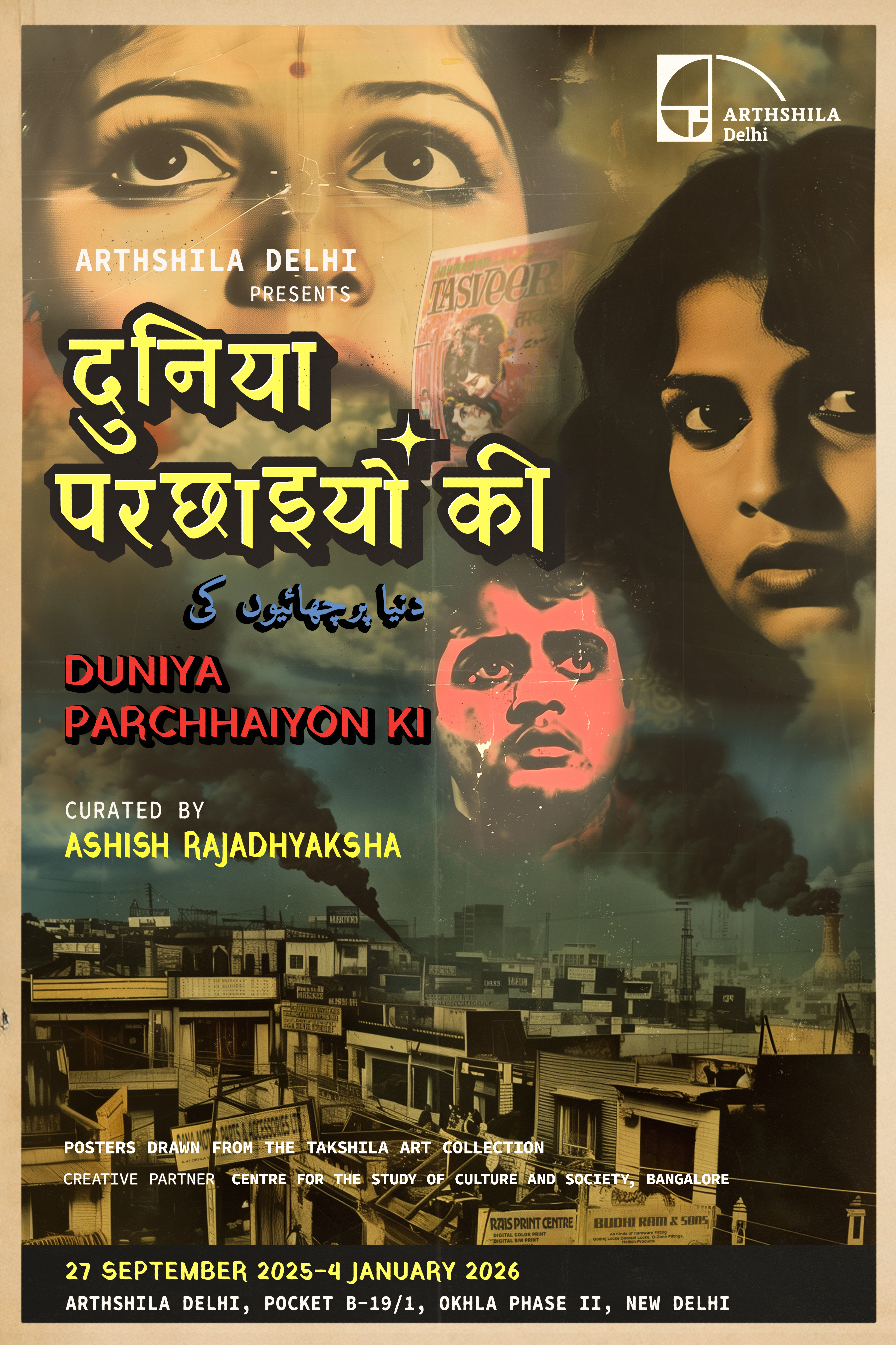
You must be logged in to post a comment.